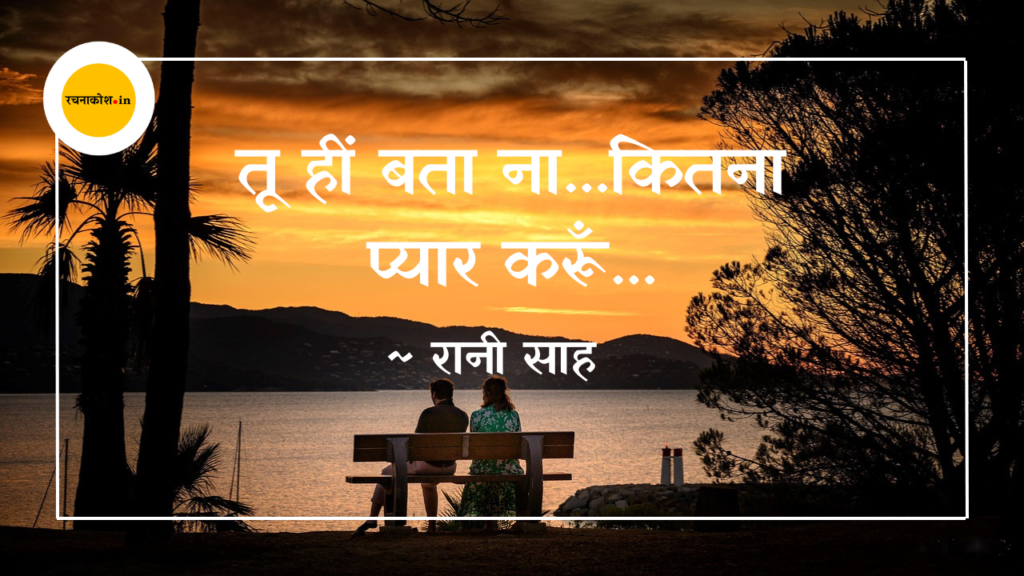दिल के किसी कोने में अकेला बैठा रेडियो अपने कवच कुंडल की तलाश में व्याकुल घूमता हुआ।
हमें वो दौर भी याद है जब शाम के वक्त पिताजी रेडियो सुनते हुए अपने मोटरसाइकिल को साफ किया करते थें। रूम के किसी कोने में बैठ कर मेरे जैसा एक छोटा बच्चा यही सोचा करता था कि इस छोटे से बक्से में से “हेलो फरमाइश” जैसी आवाज़ और फिर गाना कैसे बजने लगता है। हमें वो दौर भी याद है जब इस छोटे से बक्से से आवाज़ आनी बंद हो जाती थी तो पिताजी कहते थे कि “बेटा जरा टॉर्च की बैटरी निकाल कर लाना…”। हमें वो दौर भी याद है जब उस छोटे से बक्से में लगे 2 गोलाकार चकरी को जोर से घुमा देने पर पिताजी चिल्लाते हुए ये कहते थे “कहाँ से ये नालायक पैदा हो गया है, रेडियो खराब कर देगा…”। हमें वो दौर भी याद है जब एक बार भारत – पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के वक्त गाँव में एक चाय दुकान पर उस छोटे से बक्से को सुनने के लिए भीड़ इक्कठी हो गयी थी। ऐसे अनगिनत भूली – बिसरी यादों को समेटे कई दशक निकल गए लेकिन रेडियो अब भी दिल के किसी छोटे से कोने में विराजमान है। पाठकों के जहन मे ये सवाल जरूर आया होगा – दिल के किसी छोटे से कोने में क्यों ? इसपे आगे जरूर बात करेंगे।
सन 2000 के दशक में जन्मा हर वो बच्चा गुज़रते वक्त के साथ काश ये समझ पाता कि उस छोटे से बक्से को ‘रेडियो’ कहा जाता है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी रहती है। बदलते वक्त के साथ रंगीन टेलीविजन और प्राइवेट चैनलों की भरमार के बीच रेडियो की हाल कर्ण वाली हो चली थी। कवच कुंडल वापस लेने के बाद जिस प्रकार युद्ध के मैदान में कर्ण निर्बल प्रतीत हो रहा था। कुछ दशक पहले टेलीविजन की होड़ और अब के दौर में सोशल मीडिया के मैदान में रेडियो भी अपने कवच कुंडल पाने की तलाश में व्याकुल घूम रहा है।
बरहाल एक नज़र उस स्वर्णिम दौर पर डालते है जब रेडियो और रेडियो की बैटरी जैसे शब्द इस शोर्यमण्डल में गूँजने लगें। 1880 में इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक तरंग के खोज के साथ जब महज 16 साल की उम्र में गुलयेल्मो मार्कोनी ने 1890 में रेडियो का आविष्कार किया तब उन्हें कहाँ पता था की रेडियो की पहुँच देश के 99.19% जनसंख्या तक पहुँच जाएगी। 23 दिसंबर 1900, जब कनाडाई आविष्कारक रेजिनाल्ड ए. फेसेन्डेन ने विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से ऑडियो भेजने का अविष्कार किया तब ये कहा पता था कि कलयुग का एक दौर ऐसा आएगा जब रेडियो को मोबाइल पर सुनने की तकनीक का इज़ाद हो जाएगा। 24 दिसम्बर 1906 की शाम कनाडाई वैज्ञानिक ‘रेगिनाल्ड फेसेंडेन’ ने जब अपना वॉयलिन बजाया और अटलांटिक महासागर में तैर रहे तमाम जहाजों के रेडियो ऑपरेटरों ने उस संगीत को अपने रेडियो सेट पर सुना तब ये कहा पता था कि रेडियो पर श्रोता भी अपने फरमाइशी गीत सुन पाएंगे। 1918 में ‘ली द फोरेस्ट’ ने न्यू यॉर्क के हाईब्रिज इलाके में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरु किया तब ये कहाँ पता था कि एक वक्त के बाद भारत देश मे ‘आकाशवाणी’ के 450 केंद्र संचालित होंगे। नवंबर 1941 को ‘सुभाष चंद्र बोस’ ने रेडियो जर्मनी से भारतवासियों को संबोधित किया तब ये कहाँ पता था कि जब इकीसवीं सदी में लोग रेडियो से दूर हो चुके रहेंगे, फिर कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो रेडियो पर ‘मन की बात’ करेगा।
सन 1936, भारत में सरकारी ‘इम्पेरियल रेडियो ऑफ इंडिया’ की शुरुआत और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का आकाशवाणी बन जाना मानो तलाब में किसी खिले कमल की तरह दिखाई पड़ता है। एक दौर को याद करें तो ‘हवामहल’, ‘जयमाला’, ‘संगीत सरिता’, ‘भूले बिसरे गीत’, ‘चित्रलोक’, ‘छायागीत’ जैसे कार्यक्रम हमेशा के लिए सदाबहार बन गए। बदलते वक्त के साथ भारत मे एफएम प्रसारण की शुरुआत 1977 में हुई और वर्ष 2001 के बाद एफएम प्रसारण का निजीकरण तेजी से हुआ। इसके फलस्वरूप भारत का पहला निजी एफएम रेडियो स्टेशन ‘रेडियो सिटी’ बैंगलोर, 3 जुलाई 2001 को शुरू हुआ। समय के साथ रेडियो को और सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2006 में भारत सरकार ने सामुदायिक रेडियो दिशा – निर्देश की अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के तहत गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाजिक संगठन, शिक्षा संस्थान को सामुदायिक रेडियो स्टेशन संचालित करने की अनुमति मिली। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान में 200 से ज्यादा सामुदायिक रेडियो स्टेशन देश मे संचालित हो रहें हैं।
कहतें हैं परिवर्तन संसार का नियम है। लेकिन इस परिवर्तन रूपी शब्द ने रेडियो को कुछ ज्यादा ही संकट में डाल दिया। एक तरफ जहाँ दुनिया 5G और सोशल मीडिया की चकाचौंध में उलझती जा रही है, वहीं रेडियो अब बस दिल के किसी कोने में अकेला बैठा नज़र आता है। वापस हम उस सवाल पर आते हैं जिसे मैंने ऊपर में छोड़ दिया था। रेडियो आज अकेला क्यों है ? क्या ये सवाल हम अपने अंतरात्मा से कर पाएंगे ? क्या इस सवाल का जवाब आज के आधुनिक लोग दे पाएंगे ? इसपे विचार कीजियेगा जरूर।